भारत की वायुसेना ने दशकों से हर मोर्चे पर आकाश में अपनी श्रेष्ठता साबित की है — चाहे वो 1965 हो, 1971, 1999 का कारगिल युद्ध या वर्त्तमान में जारी ऑपरेशन सिन्दूर. लेकिन आज, जब भारत एक नए सामरिक युग में प्रवेश कर रहा है, वायुसेना एक जटिल संकट का सामना कर रही है जो न सिर्फ उसकी क्षमता, बल्कि भविष्य की युद्ध-नीति को प्रभावित करता है. स्क्वाड्रनों की संख्या जरूरत से कम है, और पुराने विमान अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं. वायुसेना के पास तय 42 क्षमता से लगभग 11 से 12 स्क्वाड्रन कम हैं. एक ऐसे दौर में, जब देश दो फ्रंट पर युद्ध की संभावना से जूझ रहा है, हर स्क्वाड्रन, हर उड़ान, और हर पायलट का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है, यह केवल 11 स्क्वाड्रन का अंतर नहीं है, बल्कि 200 से अधिक लड़ाकू विमानों की जरूरत को दर्शाती है.
यह संकट अचानक नहीं आया. यह उस दीर्घकालिक नीति, धीमे रक्षा अधिग्रहण और घरेलू उत्पादन की सीमाओं का परिणाम है, जिसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं. जनवरी 1950 में, जब भारत गणराज्य बना, उस समय IAF में 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे. 1962 में भारतीय वायुसेना में 23, 1965 में 32 और 1971 में 36 स्क्वाड्रन थी. भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 1996 में 41 तक पहुंचकर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन उसके बाद यह संख्या लगातार घटती चली गई 2003 में 38, 2013 में 35, 2018 में 33 और आज या संख्या घटकर 31 पर आ चुकी है.
आज़ादी के बाद की योजनाओं में IAF के लिए 20 स्क्वाड्रन की मांग की गई, जिसमें से 15 (11 लड़ाकू स्क्वाड्रन) की दिसंबर 1953 तक मंज़ूरी मिल गई थी. पाकिस्तान के पश्चिमी देशों से जुड़ने और चीन के खतरे के उभरने के बाद, IAF ने अपनी मांग बढ़ा दी. 1959 में कुल 23 स्क्वाड्रन और 1961 में 33 स्क्वाड्रन को मंजूरी मिली.
मध्य-साठ के दशक में, टाटा कमेटी ने भारत के लिए 64 स्क्वाड्रन वाली वायु सेना की सिफारिश की थी. उस समय खतरा कम था और तकनीक अपनी शुरआती फेज में थी, तब भारत सरकार ने 39.5 फाइटर स्क्वाड्रन की सेना को मंजूरी दी, जिसमे सितंबर 2000 में IAF के ‘विजन 2020’ के आने तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ‘विजन 2020’ में IAF द्वारा 55 स्क्वाड्रन की सिफारिश की गई थी. इसके बाद, सरकार ने 13वीं प्लान (यानी 2027) तक 42-45 स्क्वाड्रन की सेना को मंजूरी दी. वहीं दूसरी तरफ, स्वीकृत स्क्वाड्रन क्षमता की वृद्धि भी बेहद धीमी रही — 1962 में जहां यह संख्या 35 थी, वहीं 2012 तक बढ़कर सिर्फ 42 तक ही पहुंच सकी.
भारतीय वायुसेना के लिए 42 स्क्वाड्रनों की क्षमता तय की गई है, लेकिन फिलहाल यह घटकर सिर्फ 31 स्क्वाड्रन रह गई है, यानी देश को 11 स्क्वाड्रनों की कमी झेलनी पड़ रही है, यह कमी कई वजहों से आई है — जैसे पुराने विमानों (जैसे MiG-21) का रिटायर होना, नए स्वदेशी विमानों (जैसे Tejas Mk1A और AMCA) की धीमी गति से टेस्टिंग, चयन और तैनाती, और विदेशी खरीद (जैसे Rafale) की सीमित संख्या.
भारत इस समय एक जटिल स्थिति में फंसा हुआ है — पुराने विमान जैसे MiG-21 और Jaguar अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, और अब आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं. हाल ही में राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे दो पायलट शहीद हो गए. यह पिछले कुछ महीनों में तीसरा Jaguar क्रैश था — इससे पहले अप्रैल में गुजरात और मार्च में अंबाला में ऐसे ही हादसे हो चुके हैं. तेजस Mk1A का उत्पादन गति नहीं पकड़ पाया है, AMCA जैसी परियोजनाएँ अभी विकास चरण में हैं, और विदेशी विकल्पों पर हमारी निर्भरता सीमित हो गई है — चाहे वह Rafale हो या अन्य मल्टी-रोल फाइटर जेट. ऐसे में आज भारतीय वायुसेना कॉम्बैट रोल के लिए लगभग पूरी तरह Su-30MKI और 36 राफेल (दो स्क्वाड्रन) पर ही निर्भर रह गई है.
सरकार ने इस अंतर को नजरअंदाज़ नहीं किया है. जब तक नए लड़ाकू विमान स्क्वाड्रनों में नहीं आते, तब तक भारत ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स पर फोकस करके वायु सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. यही वह रणनीतिक ‘फायरवॉल’ है, जिसके सहारे भारत ने दुश्मन की किसी भी पहली लहर को आसमान में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित की है.
यह प्रयास सिर्फ सिद्धांत नहीं रहा — मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बना. पाकिस्तान द्वारा भेजे गए सैकड़ों ड्रोन और क्रूज़ मिसाइलों को बिना एक भी फाइटर जेट उड़ाए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में ही नष्ट कर दिया. S-400, Akash, Barak-8, QRSAM और Akashteer जैसे सिस्टम्स ने यह दिखा दिया कि भारत की वायु रक्षा अब केवल रिएक्टिव नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट और प्रोएक्टिव हो चुकी है.
Akashteer जैसे स्वदेशी सिस्टम आज इस बदलाव का चेहरा बन चुके हैं — यह तकनीक केवल मिसाइल लॉन्च नहीं करती, बल्कि पूरे युद्धक्षेत्र को जोड़ती है, निर्णय लेती है और खतरे को पहचानकर स्वत: कार्रवाई करती है. यही बदलाव भारत की वायु सुरक्षा को एक नये स्तर तक ले जा रहा है.
लेकिन सवाल यही है — क्या यह इंतज़ाम हमारी आक्रामक क्षमता का विकल्प बन सकता है?
उत्तर है — नहीं. एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते. वे आक्रामक रणनीति का स्थान नहीं ले सकते. युद्ध केवल रक्षात्मक दीवारों से नहीं, बल्कि निर्णायक और रणनीतिक प्रहारों से जीते जाते हैं. इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास आधुनिक, तेज़, स्टील्थ-सक्षम और मल्टी-रोल फाइटर जेट हों — जो न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें, बल्कि दुश्मन की गहराई में घुसकर रणनीतिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकें.
आज की एयर डिफेंस रणनीति निश्चित रूप से किफायती और बुद्धिमानी से प्रेरित है. एक फाइटर जेट की कीमत जहां ₹700–800 करोड़ तक होती है, वहीं एक एयर डिफेंस बैटरी उसी लागत में कई टारगेट को कवर करने में सक्षम होती है. लेकिन यह भी सत्य है कि केवल किफायत से युद्ध नहीं जीते जाते. जब बात आत्मनिर्भर भारत की हो, तो Project Kusha और Akashteer जैसे सिस्टम एक मजबूत आधार बनाते हैं — लेकिन उनकी भूमिका सीमित है.
भारत अगर केवल डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर रहेगा, तो वह हमेशा रिएक्टिव पोजिशन में रहेगा — यानी दुश्मन के पहले वार के बाद ही प्रतिक्रिया देगा. इस नीति से ‘स्ट्राइक कैपेबिलिटी’ कमज़ोर पड़ती है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स आज के लिए एक चतुर और आवश्यक रणनीति हैं — वे वक़्त दिलाते हैं, रक्षा मजबूत करते हैं, और दुश्मन के मंसूबों को विफल करते हैं. लेकिन दीर्घकालिक सुरक्षा, वायु वर्चस्व और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए लड़ाकू विमानों की पूर्ण क्षमता बहाल करना ही एकमात्र स्थायी उपाय है.
भारत को तीन मोर्चों पर समानांतर रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता
1. फाइटर जेट स्क्वाड्रनों की संख्या को शीघ्रता से बढ़ाना – Su-30MKI, Rafale की संख्या बढ़ाई जाए, Tejas Mk1A को तेज़ी से प्रोडक्शन में लाया जाए, AMCA जैसे प्रोजेक्ट को फास्ट-ट्रैक किया जाए और नई मल्टी-रोल विदेशी फाइटर खरीद पर भी जल्द निर्णय हो.
2. एयर डिफेंस नेटवर्क को देशभर में जोड़ना – Akashteer जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम पूरे थलसेना और वायुसेना में इंटीग्रेट किए जाएं, उत्तरी सीमाओं, द्वीप क्षेत्रों और रणनीतिक ठिकानों को डबल कवर दिया जाए.
3. Airborne Surveillance और Drone Warfare में निवेश – AEW&C, DRDO Netra और ड्रोन्स की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है. स्वार्म, लोटरिंग, Surveillance ड्रोन की एक आधुनिक फाॅर्स रेडी करना होगा.
ऑपरेशन सिन्दूर में ये सिस्टम भारतीय वायु रक्षा की नई रीढ़ बनकर उभरे हैं
भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के प्रयास में सरकार और रक्षा अनुसंधान संगठनों ने कई अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती की है — ये ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल को सीमाओं में दाखिल होने से पहले ही हवा में खत्म कर सकते हैं. मौजूदा हालात में, जब लड़ाकू विमानों की संख्या रणनीतिक ज़रूरतों से कम है, तब ये सिस्टम भारतीय वायु रक्षा की नई रीढ़ बनकर उभरे हैं.
S-400 ट्रायंफ: दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक, रूस से आयातित S-400, एक साथ कई टारगेट्स को 400 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है. यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन जैसे सभी प्रकार के हवाई खतरों से निपट सकता है. भारत को अब तक इसकी तीन यूनिट मिल चुकी हैं, और शेष दो 2025 के अंत तक अपेक्षित हैं.
Akashteer (आकाशतीर): यह कोई साधारण एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि युद्ध की पूरी सोच को बदलने वाला प्लेटफॉर्म है. यह सेना को एक साझा, वास्तविक समय की हवाई तस्वीर देता है, जिसमें कंट्रोल रूम, रडार और गन सिस्टम आपस में पूरी तरह समन्वय में काम करते हैं. आकाशतीर ऑटोमेटिक है — खतरे की पहचान, ट्रैकिंग और जवाबी कार्रवाई में इंसानी देरी की ज़रूरत नहीं. यह सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह कारगर साबित हुआ, जहाँ पाकिस्तान द्वारा भेजे गए सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल को सटीकता से मार गिराया गया.
आकाश मिसाइल सिस्टम: DRDO द्वारा विकसित यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली (SAM) भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल है. इसकी मारक रेंज 25–30 किमी तक है और यह 18 किमी की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट्स को भी भेद सकती है. इसमें मल्टी फंक्शन रडार, सेंट्रल एक्विज़िशन रडार और फायर कंट्रोल यूनिट्स हैं, जो इसे बहु-आयामी खतरे से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं.
Barak-8: भारत और इज़राइल के संयुक्त विकास का नतीजा — Barak-8 एक अत्यधिक उन्नत, लंबी दूरी की SAM प्रणाली है. यह दुश्मन के विमानों, हेलिकॉप्टरों, मिसाइलों और ड्रोन को 100 किमी दूर से भी पहचान कर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखती है. इसकी एक्टिव रडार सीकर और वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी इसे विशेष बनाती हैं. इसका 360-डिग्री कवरेज इसे नौसेना और थल सेना दोनों के लिए आदर्श बनाता है.
SPYDER (Surface-to-Air PYthon and DERby): इस इज़रायली प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है — “रेड-टू-फायर” रेस्पॉन्स. यह किसी भी हवाई खतरे को चंद सेकंड में पहचानकर तुरंत जवाब दे सकता है. इसके अलग-अलग वर्जन (SR, MR, LR, ER, और All-in-One) इसकी उपयोगिता को कम से लेकर बहुत लंबी दूरी तक फैला देते हैं. इसे दुनिया की 8 बड़ी सेनाएं अपना चुकी हैं — और इसकी विश्वसनीयता को कई युद्धाभ्यासों में परखा जा चुका है.
QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile): यह एक अत्यधिक गतिशील, शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे खासतौर पर बख्तरबंद फौजों के लिए डिजाइन किया गया है. यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों, हेलिकॉप्टरों और फाइटर जेट्स को तत्काल पहचानकर निष्क्रिय कर सकता है. हाल ही में भारत सरकार ने इसके तीन रेजीमेंट की खरीद के लिए ₹36,000 करोड़ का सौदा किया है, जो इस सिस्टम की रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है.

 6 hours ago
6 hours ago


)
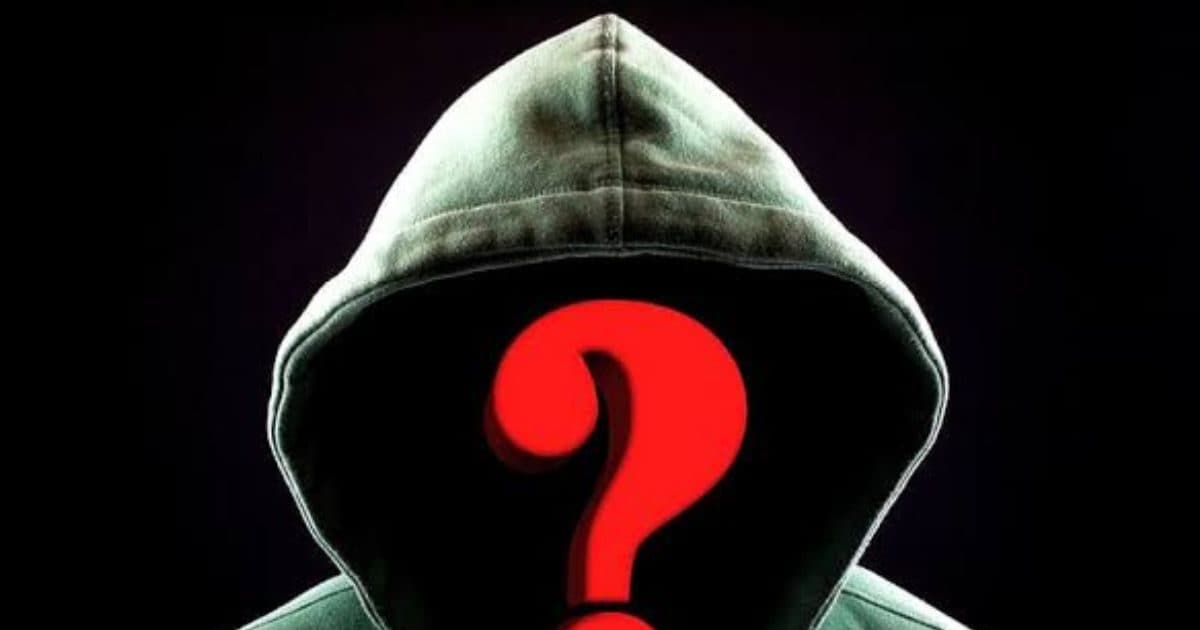





)






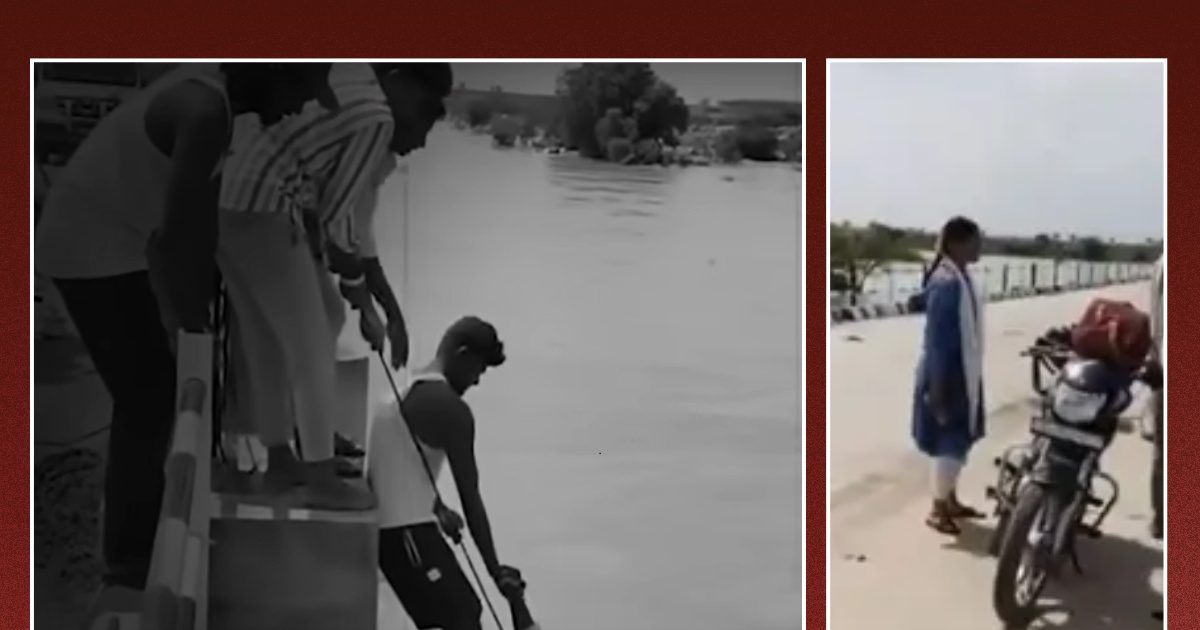
)
