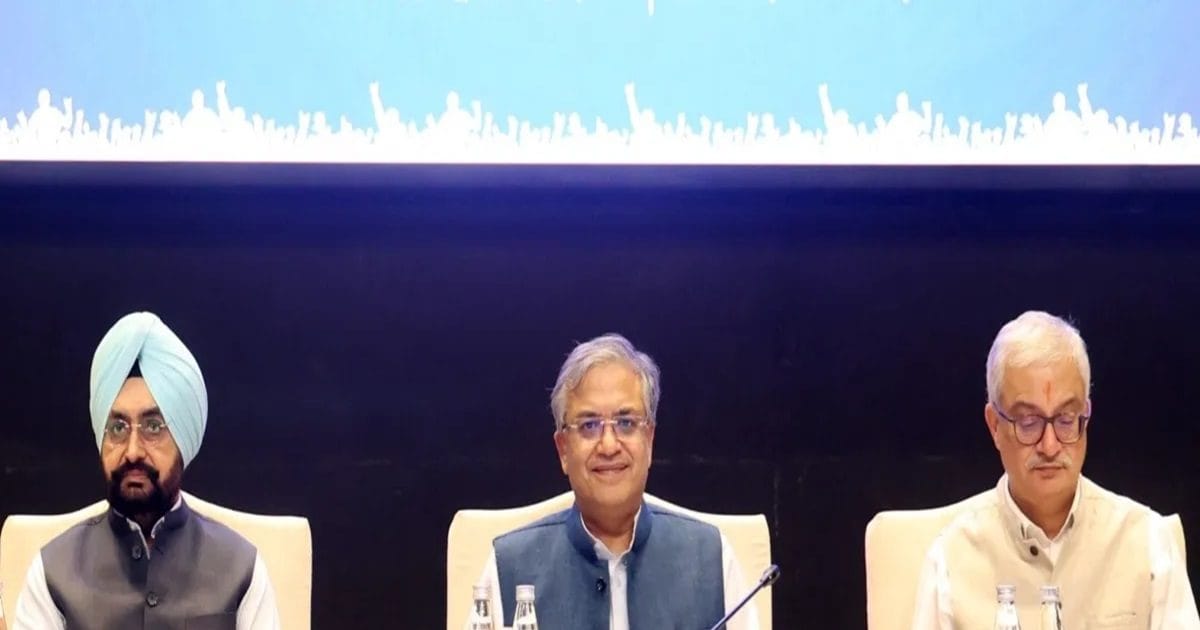ये बात एकदम सही थी कि कश्मीर के महाराजा हरिसिंह शुरू में किसी भी हालत में भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे. अक्सर कहा जाता है कि अगर महाराजा हरिसिंह ने अगस्त 1947 में ही भारत से विलय कर लिया होता तो शायद पाकिस्तान को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही कश्मीर की स्थिति आने वाले सालोंसाल इतनी पेचिदा बनी रहती. इस दौर में लिखी गई किताबों में इसका जिक्र है कि भारत की तमाम कोशिश के बाद भी महाराजा ने भारत में शुरू में विलय स्वीकार नहीं किया. हां,वो पाकिस्तान में भी किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहते थे.
ब्रिटिश भारत के विभाजन यानि 15 अगस्त 1947 के बाद 565 रियासतों को यह अधिकार मिला था कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों, या स्वतंत्र रहें.कश्मीर भी इन्हीं रियासतों में से एक थी. यह रियासत धार्मिक रूप से जटिल थी. यहां जनसंख्या की करीब 77% आबादी मुसलमानों की थी. इसके शासक हिदू राजा हरिसिंह थे. विशाल कश्मीर रियासत भौगोलिक रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी थी.
क्या थी भारत की आजादी के बाद महाराजा की नीति
हरिसिंह की नीति थी- ना भारत और ना ही पाकिस्तान. महाराजा हरिसिंह का रुख शुरू से स्पष्ट था – “कश्मीर न भारत के साथ जाएगा, न पाकिस्तान के साथ.”
इस नीति का उल्लेख कई स्रोतों में मिलता है. भारत सरकार के तत्कालीन सचिव और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के दाएं हाथ कहे जाने वाले वी.पी. मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया (Integration of the Indian States, 1956) में लिखते हैं, महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे और मानते थे कि भारत-पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाकर वह अपने राज्य की स्थिति मजबूत रख सकते हैं.
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विन फ्रीडम (India Wins Freedom, 1959) में लिखा, हरिसिंह पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाने का सपना देख रहे थे.
हरिसिंह का मानना था कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो भौगोलिक रूप से सुंदर, रणनीतिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है. उनका सपना था कि यह एक स्वतंत्र तटस्थ राज्य बने, जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों से मित्रवत संबंध हों.
महाराजा के इस विचार का उल्लेख इतिहासकार अलस्टेयर लैम्ब ने अपनी किताब कश्मीर – ए डिस्पुटेड लीगेसी (Kashmir: A Disputed Legacy, 1991) में किया है. वह लिखते हैं, वह दोनों देशों से दोस्ती रखते हुए खुद को किसी एक के अधीन नहीं करना चाहते थे.
क्या था आखिर इसकी वजह
ये सवाल उठता है कि महाराजा हरिसिंह आखिर ऐसा क्यों चाहते थे. क्यों वह भारत और पाकिस्तान के बीच अपनी विशाल रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे. दरअसल कश्मीर की राजनीति उस समय शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द-गिर्द घूम रही थी. शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता जनता में बहुत थी. वह कांग्रेस के नजदीक थे.
महाराजा को लगता था कि अगर उन्होंने भारत से विलय किया तो “कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला मिलकर उनका सिंहासन छीन लेंगे.”
वी.पी. मेनन लिखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के पत्राचार ( Archives of India) में भी दर्ज है कि हरिसिंह ने दिल्ली से भेजे अपने संदेश में कहा था, अगर मैने भारत से विलय किया तो मैं अपना ताज शेख अब्दुल्ला के हाथों गंवां दूंगा. इसलिए उन्होंने भारत से दूरी बनाए रखी.
हरिसिंह एक हिंदू डोगरा राजा थे. उनकी रियासत में बहुमत मुस्लिम था. उन्हें डर था कि भारत में शामिल होने पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनके शासन को “सांप्रदायिक” कहा जाएगा. पाकिस्तान उन्हें “हिंदू राजा मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है” के रूप में प्रचारित करेगा.
इतिहासकार और तब संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि जोसफ कॉरबेल अपनी किताब डेंजर इन कश्मीर (Danger in Kashmir, 1954) में लिखते हैं, हरिसिंह को डर था कि अगर वो भारत में विलय करते हैं तो उन पर ये आरोप लगेगा कि मुस्लिम बहुत राज्य होते हुए भी उन्होंने इसे जबरदस्ती भारत में मिलवाया.
महाराजा ने भारत और पाकिस्तान को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भेजा
जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए तब महाराजा हरिसिंह ने दोनों देशों को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भेजा. दरअसल इसका मतलब ये था कि जब तक कि वो कोई फैसला नहीं लेते तब तक उनकी डाक, रेल, टेलीफोन, व्यापार, संचार व्यवस्थाएं पहले की तरह दोनों बने नए देशों से संचालित की जाती रहें, जैसा ब्रिटिश भारत में होता था.
मुख्य तौर पर “स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट” ये कहता था, “जब तक आप किसी देश के साथ औपचारिक रूप से नहीं जुड़ते, तब तक प्रशासनिक सेवाएं, व्यापार, और संचार व्यवस्था पहले जैसी चलती रहेगी.”
इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार किया. पाकिस्तान ने उसी दिन यानि 15 अगस्त 1947 को महाराजा को ये संदेश भेजा, पाकिस्तान सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर राजी है. इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की डाक, टेलीफोन और सप्लाई सेवाएं पहले की तरह चलाएगा, राज्य की स्वतंत्र स्थिति बरकरार मानी जाएगी और दोनों के बीच कोई सैन्य या राजनीतिक दखल नहीं होगा.
भारत ने जवाब में कहा कि “हम पहले इस प्रस्ताव की शर्तें देखना चाहेंगे.” यानी भारत ने तुरंत इस समझौते को स्वीकार नहीं किया. हालांकि यह एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज़ नहीं था, लेकिन इसकी “व्यवहारिक” शर्तें कुछ इस तरह थीं –
1. डाक और तार सेवाएं – पाकिस्तान की एजेंसियां इन्हें पहले की तरह चलाती रहेंगी.
2. परिवहन – पाकिस्तान के माध्यम से आने-जाने वाली सड़कों और रेल मार्गों को खुला रखा जाएगा.
3. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति – जैसे पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, नमक आदि पाकिस्तान की ओर से आते रहेंगे.
4. व्यापार – व्यापारिक लेन-देन पूर्व व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा.
5. कानूनी स्थिति – किसी भी पक्ष को राज्य की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा.
पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया
पाकिस्तान ने एक ओर तो स्टैंडस्टिल समझौते को तुरंत स्वीकार कर लिया था लेकिन एक महीने बाद ही सितंबर 1947 से, उन्होंने पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ जाने वाले तेल, खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी. डाक और टेलीफोन लाइनों को भी बाधित किया गया. यह एक “आर्थिक नाकेबंदी” थी ताकि महाराजा पर दबाव बनाया जा सके.
फिर कबायली हमलावरों को घुसा दिया
22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना की मदद से कबायली हमलावर कश्मीर में घुस गए. यानी जिस समझौते का मकसद “अमन और स्थिरता” था,
पाकिस्तान ने उसी का इस्तेमाल हमले की तैयारी के लिए किया. वास्तव में पाकिस्तान ने इसी समझौते का इस्तेमाल बाद में कबायली हमले की तैयारी में किया
जम्मू-कश्मीर की सरकार के वर्ष 1948 के श्वेत पत्र में लिखा गया, जम्मू-कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया. पहले पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया और फिर इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया. आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी और कबायली हमलावरों से हमला शुरू करा दिया.
वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में लिखा, पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर का स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट घातक साबित हुआ. उसने दोस्ती का ढोंग तो जरूर भरा लेकिन जम्मू-कश्मीर पर कंट्रोल करने के लिए संचार और आपूर्ति पर कंट्रोल शुरू कर दिया.
जोसेफ कोरबेल ने किताब डेंजर इन कश्मीर में लिखा, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान को एक हथियार मिल गया. उसने दरअसल इसके जरिए महाराजा को सुरक्षा देने का झूठा भरोसा दिया.
माउंटबेटन ने लिखा, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट मंजूर करके पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूदगी बढ़ाई जो बात में कश्मीर के लिए घातक साबित हुई.
कानूनी तौर पर स्टैंडस्टिल का मतलब
कानूनी दृष्टि से स्टैंडस्टिल का अर्थ होता है, “एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष सहमत हों कि किसी मौजूदा व्यवस्था में तब तक कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कोई नया अनुबंध या निर्णय नहीं ले लिया जाता.” यानी ऐसा “status quo” जिसमें जैसी स्थिति है, वैसी ही रहे. स्टैंडस्टिल इसे ही बनाए रखने का औपचारिक तरीका था.
तब कश्मीर की भौगोलिक निर्भरता की क्या स्थिति थी
कश्मीर की मुख्य सड़कें, रेल और संचार मार्ग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर गुजरते थे. भारत के साथ कोई सीधा सड़क या रेल संपर्क नहीं था. हरिसिंह को डर था कि भारत से जुड़ने पर पाकिस्तान आर्थिक नाकेबंदी कर देगा. जो बाद में हुआ भी. इतिहासकार पॉल वॉलेस ने अपनी किताब पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन कश्मीर (Political Development in Kashmir,1980) में लिखा, पाकिस्तान पर आर्थिक निर्भरता ने हरि सिंह को सतर्क किया हुआ था. वह मान रहे थे कि तटस्थ रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है.
जब कबायलियों का हमला हुआ तो महाराजा की “तटस्थ रहने” की नीति ने उन्हें अचानक असहाय बना दिया. अब उनके पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. तब जाकर 26 अक्टूबर को उन्होंने Instrument of Accession पर साइन किए. ये भी कहा जाता है कि महाराजा हरिसिंह एक महत्वाकांक्षी लेकिन भ्रमित शासक थे. उनकी सोच यह थी कि “अगर मैं भारत या पाकिस्तान किसी से नहीं जुड़ता, तो दोनों मेरे साथ अच्छे संबंध रखने को मजबूर रहेंगे.” लेकिन यह नीति बहुत जल्द उलटी पड़ी. भारत ने स्पष्ट कहा, “पहले विलय करो, तभी मदद मिलेगी.” इस तरह महाराजा की “तटस्थता” की नीति ही आखिरकार उन्हें भारत की गोद में ले आई पर तब तक कश्मीर की कहानी में “विवाद” का बीज बोया जा चुका था.
27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ
27 अक्टूबर की सुबह पहला भारतीय विमानों का काफिला श्रीनगर हवाईअड्डे पर उतरा. इन विमानों में एक सिख रेजिमेंट के सैनिक थे. उन्होंने श्रीनगर की रक्षा की और बारामुला की ओर बढ़ते कबायली हमले को रोका. यहीं से पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध (1947–48) शुरू हुआ.

 4 hours ago
4 hours ago



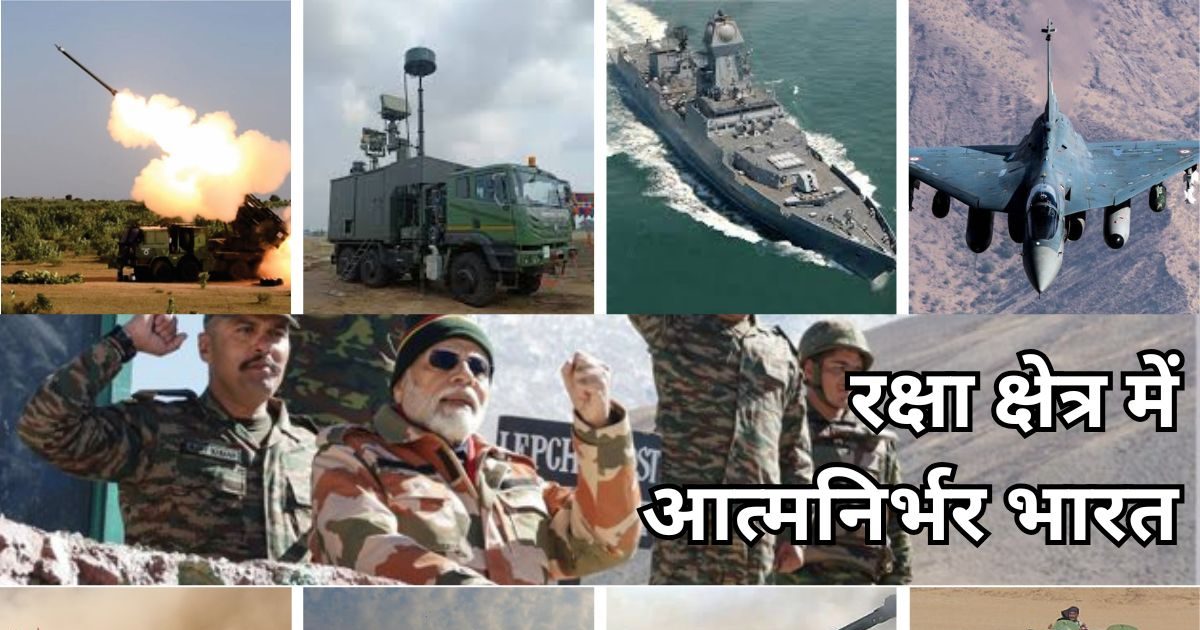

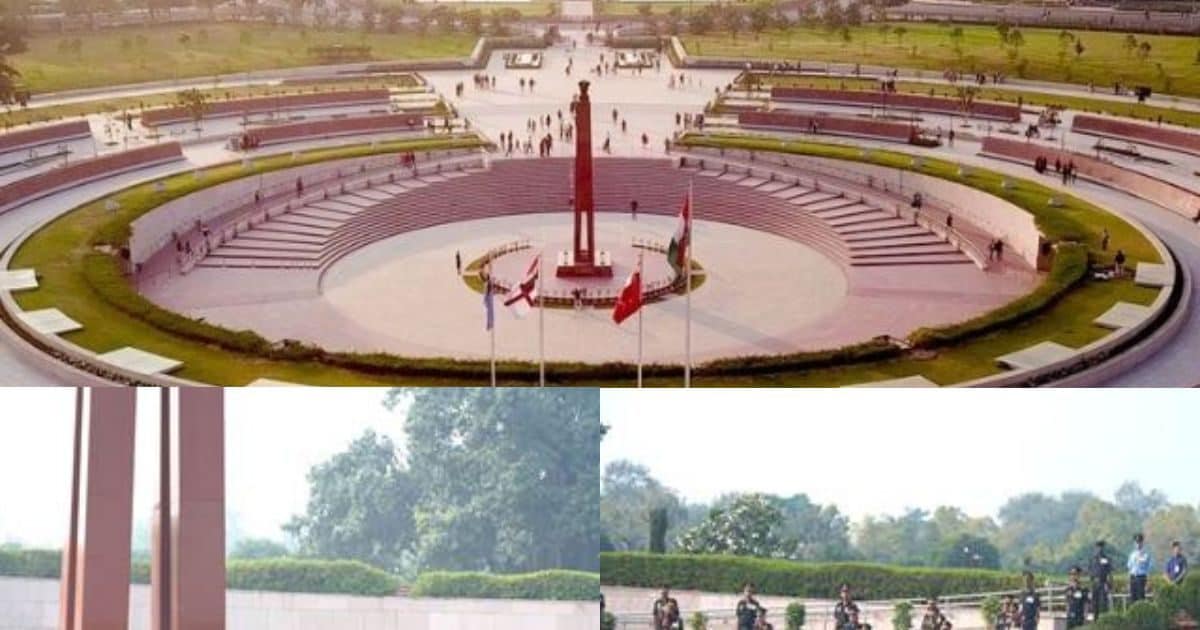

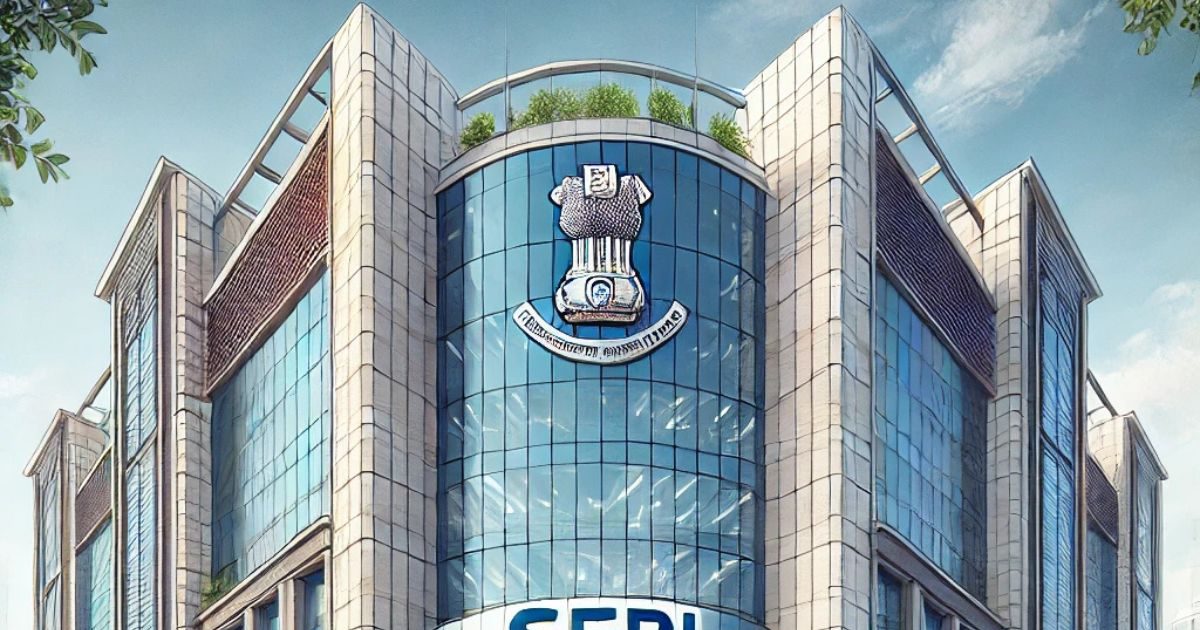





)
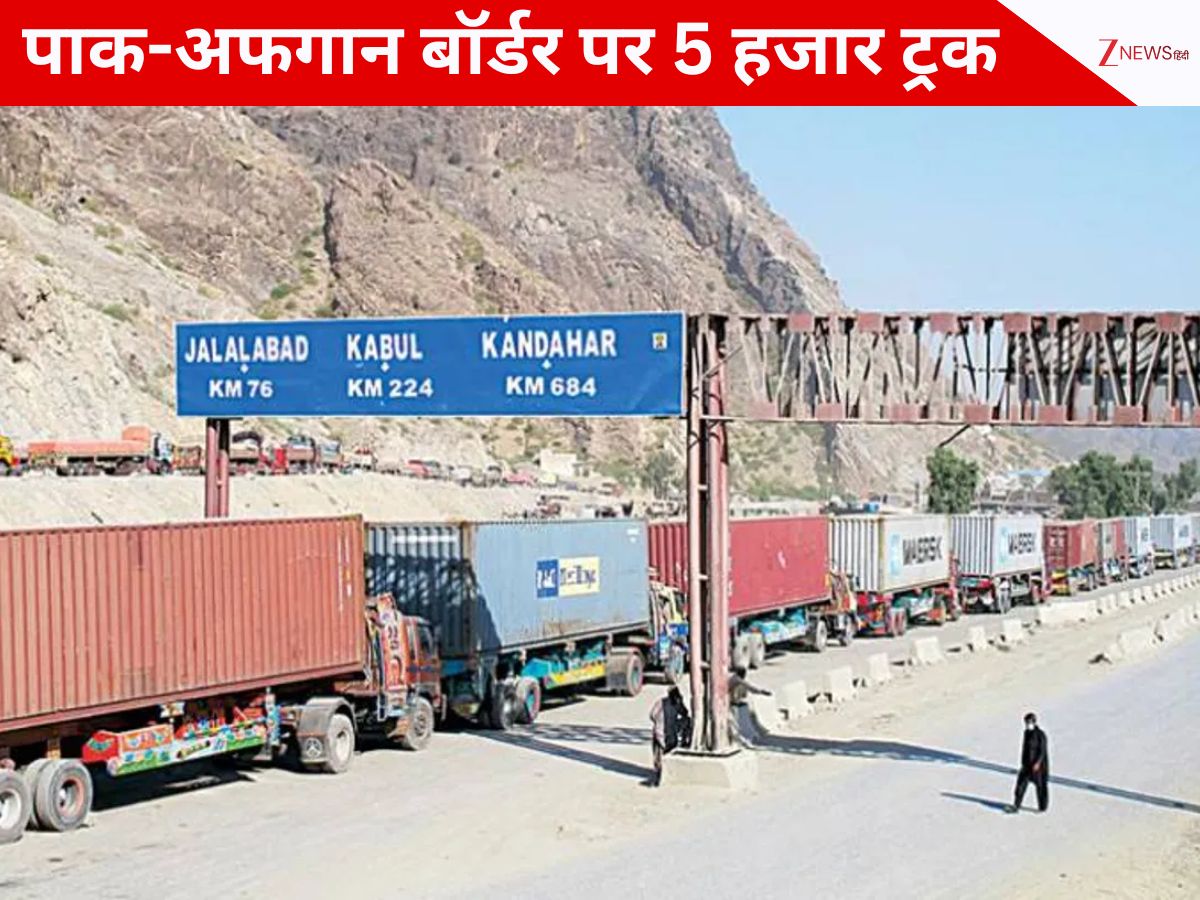)